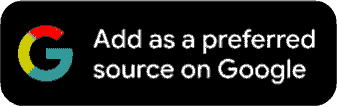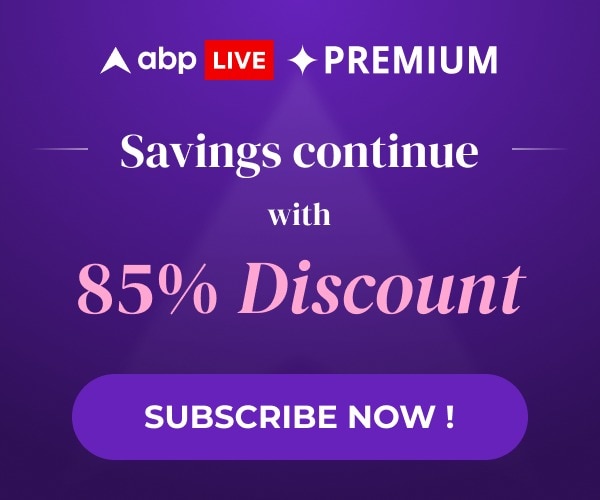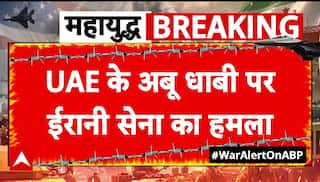आलोचनात्मक विवेक के धनी थे नामवर सिंह
नामवर सिंह ने पिछली सदी के पांचवें दशक के आरंभ में लिखना आरंभ किया था. तब से लेकर अंत के बस कुछ बरस पहले तक वे हिन्दी साहित्य और समाज में लगातार 'मौजूद' रहे. उनकी जानकारी और दिलचस्पी की रेंज कमाल की थी.

नामवर सिंह कवि, कहानीकार या उपन्यासकार नहीं आलोचक थे. कहानी, उपन्यास के पाठक साहित्यिक बिरादरी के बाहर भी बहुत होते हैं, लेकिन आलोचना आम तौर से या तो लेखक पढ़ते हैं या साहित्य के विद्यार्थी. लेकिन नामवरजी के निधन पर साहित्य जगत से लेकर लोकप्रिय मीडिया तक में हलचल है. इससे वह बात इस समय भी सामने आई जो उनके जीवनकाल में बार-बार आती थी. नामवरजी की लोकप्रियता साहित्यिक हलकों तक ही सीमित नहीं है.
कारण यह कि नामवरजी साहित्यिक आलोचक होने के साथ ही लोक-बुद्धिजीवी-पब्लिक इंटेलेक्चुअल-भी थे. वे कोई जोशीले वक्ता नहीं थे, भावनाएँ जगाकर ताली बटोरना उनकी भाषण-शैली में नहीं था. वे शांत स्वर में, तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात कहते थे. विद्वता उनका सहज स्वभाव बन गयी थी, उनके भाषणों में भी कई भाषाओं के उद्धरण और कई विषयों के संदर्भ सहज ही चले आते थे. फिर उनका जबर्दस्त विट. नामवरजी के भाषण वैचारिक उत्तेजना, जानकारी, सोचने की प्रेरणा के साथ-साथ कुछ बहुत क्रिएटिव देखने-सुनने का सुख भी देते थे. वे मेरी जानकारी में , कम से कम हिन्दी में वे अकेले एकेडमिक वक्ता थे जिन्हें सुनने के लिए आम लोग, हर उम्र और हर बैकग्राउंड के, हजारों की तादाद में आते थे, ध्यान से सुनते थे, सोचते थे, हँसते भी थे, कुछ हासिल करने का सुख साथ लेकर वापस जाते थे.
उनके मेरे जैसे प्रशंसकों को यह शिकायत लगातार बनी रही कि वे लिखते कम बोलते ज्यादा हैं. दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे और हैं जो मानते हैं कि नामवरजी ने लिखने के बजाय बोलने पर ज्यादा ध्यान देकर अच्छा ही किया. इस विधि से ज्ञान और सोच आम लोगों तक पहुंचा, नामवरजी जंगम (चलते-फिरते) विद्यापीठ कहलाए. यह बात किसी हद तक सच भी है, लेकिन बड़ा सच यही है कि लिखने का कोई विकल्प नहीं. कितना भी मंजा हुआ वक्ता क्यों न हो, उसकी चेतना पर ऑडियेंस का दबाव तो पड़ता है. नामवरजी पर भी कभी-कभार सुनने वालों की मनचीती बात करने (प्लेइंग टू दि गैलेरी) के आरोप लगे.

भाषण और लेखन में बड़ा फर्क यही है कि लिखते समय लेखक अपने एकांत में हर बात पर गंभीर विचार कर सकता है. हालांकि हर लेखक करे ही, करता ही हो, यह जरूरी नहीं.
नामवरजी ने पिछली सदी के पांचवें दशक के आरंभ में लिखना आरंभ किया था. तब से लेकर अंत के बस कुछ बरस पहले तक वे हिन्दी साहित्य और समाज में लगातार 'मौजूद' रहे. उनकी जानकारी और दिलचस्पी की रेंज कमाल की थी. पृथ्वीराज रासो के जमाने से लेकर आज की हिन्दी तक के साहित्य के बारे में वे कुछ ज्ञानवर्द्धक और विचारोत्तेजक कह सकते थे.
वे मार्क्सवादी थे, साथ ही साहित्य को राजनीति का पुछल्ला भर मानने के विरोधी भी. हिन्दी के लोकवृत्त (पब्लिक स्फीयर) में उन्होंने कई बहसों, विवादों को जन्म दिया. विवाद उनके सदा के संगी थे. इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बहसों में भी बदले और कुछ व्यर्थ के ही साबित हुए. लेकिन लोकतांत्रिक, प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों के प्रति उनका समर्पण हमेशा निर्विवाद रहा.
वे आलोचक थे. यह बहुत अच्छी तरह जानने और अपने पाठकों, सुनने वालों को लगातार जताने वाले विद्वान आलोचक कि आलोचना का महत्व केवल साहित्य तक ही सीमित नहीं है. जिन्दगी के छोटे से लेकर बड़े, व्यक्तिगत, पारिवारिक से लेकर राजनीतिक तक फैसले आलोचनात्मक सोच-विचार के बाद ही लिये जाते हैं, लिये जाने चाहिए. सोच-विचार कर बोलना, काम करना यह आलोचनात्मक गतिविधि का एकदम बुनियादी रूप है, जिसके बिना रोजमर्रा का जीवन चल ही नहीं सकता. हम भावनाओं में बह कर ही जीवन जीने लगें तो किसी पल आए गुस्से के आधार पर जिन्दगी भर के रिश्ते तोड़ सकते हैं. ऐसा न हो, इसलिए सोच-विचार कर जीवन जीते हैं, केवल भावनाओं के आधार पर नहीं.
रोजमर्रा के जीवन से आगे, हमारे सामाजिक-राजनैतिक फैसले भी आलोचनात्मक विवेक के आधार पर लिये जाने चाहिएँ. आलोचना का मतलब निन्दा नहीं होता. किसी भी चीज़ को ध्यान दे रही आँखों से देखने को ही आलोचना कहते हैं, यह शब्द ही ‘लोचन’— आंख से बना है. ध्यान से देखने से ही तो सारी दार्शनिक सोच, हालात को बदलने की कोशिशें पैदा होती हैं. आलोचना साहित्य और कला की ही नहीं, जीवन मात्र की बुनियादी जरूरत है.
नामवरजी लोक-बुद्धिजीवी की भूमिका भी आलोचना के इसी महत्व के अहसास के साथ निभाते थे और संपादक की भी. कभी-कभी उनके व्यवहार में अपनी स्वयं की इस भूमिका का खंडन भी दिखता था. लेकिन कुल मिला कर वे अपने मन में स्पष्ट थे कि सब अपनी अपनी जगह ठीक टाइप का मीठापन असल में बौद्धिक आलस ही नहीं, अपंगता की सूचना देता है. मूलभूत मानवीय प्रतिमानों पर, विवेक की कसौटी पर विभिन्न सामाजिक-राजनैतिक विचारों और व्यवहारों, साहित्यिक रचनाओं को परखने और अपनी जगह तय करने का कोई विकल्प है नहीं.
आलोचक नामवर सिंह के निधन पर राजनीति से लेकर मीडिया तक हलचल है, जो स्टार-क्रेज है, उसे देखना इस बुद्धि-विरोधी समय में खासा रोमांचक है. उम्मीद है कि एक साहित्य आलोचक के प्रति यह दिख रहा यह लगाव सारे समाज को फिर से याद दिलाएगा कि राजनीति समेत ज़िन्दगी के हर हलके में भक्ति-भाव से ज्यादा ज़रूरी है—आलोचनात्मक विवेक.
(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.)